
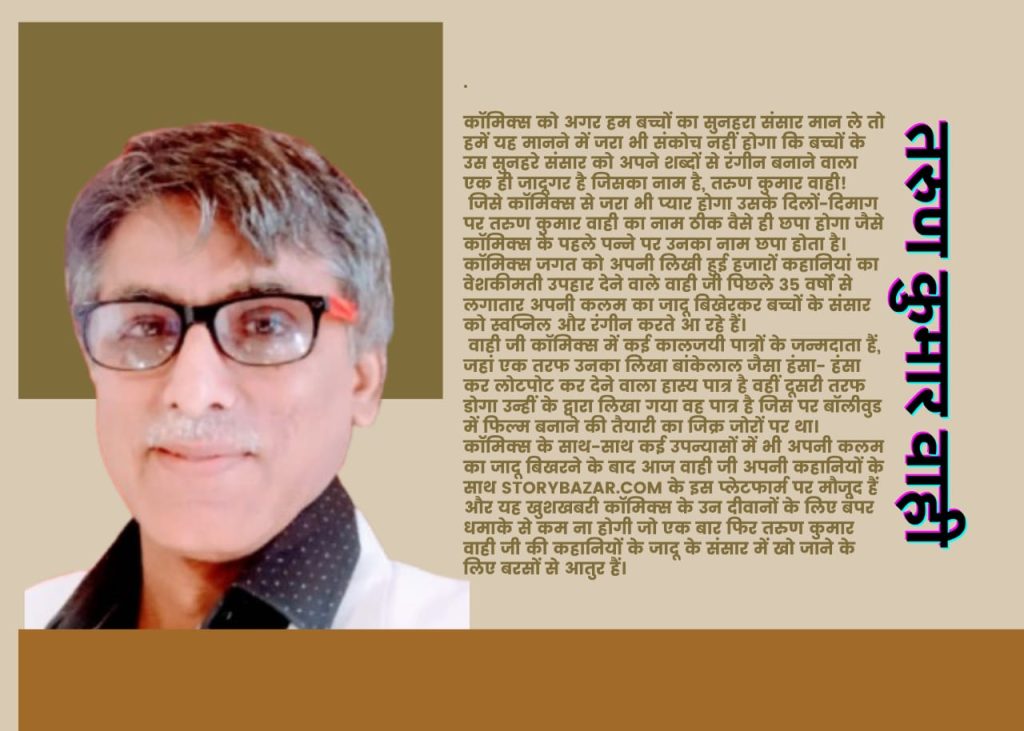
25% जिंदगी
मैं प्रिया, मैं अपनी कहानी इस छोटी सी खूबसूरत कविता से शुरू करती हूं।
“मुस्कराते हुए होंठों की खुशी, तो हर कोई देखता है, उनके पीछे छुपा दर्द अपने अलावा और, किसे दिखाई पड़ता है,
मुस्कराहट, जो बंद कमरे में अक्सर सिसक उठती है, रुआंसी हो उठती है,
जिसे कमरे की दर-ओ-दीवारें देखती हैं, या, अपने अलावा और किसे दिखाई पड़ती है,
मोमबत्ती की लौ की तरह,
कंपकंपाती एक सुख की आस, जो कभी बुझ भी जाती है, फिर जलाई जाती है,
ये जलना-बुझना, अपने अलावा,
और किसे दिखाई पड़ता है,
एक मैली चादर सा झाड़ा गया दर्द,
जो धूल के कणों की तरह हृदय के चप्पे-चप्पे पर,
उड़ता है, अपने अलावा और किसे दिखाई पड़ता है,
तपते रेगिस्तान की रेत में गिरती सूखती,
पानी की वो बूंदें कहां मिटायेंगी प्यास,
ऊपर तपता हुआ सूरज अपने अलावा,
और किसे दिखाई पड़ता है।।”
हां। बेडरूम ही वह जगह है, जहां लेटे-लेटे अक्सर सोचा करती थी।
घंटों सोच जाया करती थी।
ना सोचना चाहती तो यह भी मुमकिन था।
लेकिन! सोचा… क्यूं ना सोचूं?
तो… सोचा करती थी। सोचों को साथी जो बना लिया था। साथी से अब दिल की बातें ना करती क्या?
बातें करने के लिए मैं थी… मेरा दिल था… मेरा अपना ही दिल । “यूं हसरतों के दाग, मुहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही, और रो लिए।”
किसी शायर ने क्या खूब कहा है।
मुझे लगता है जैसे मेरे लिए ही कहा है।
‘हसरतें’ तब दाग की तरह दिखती हैं, जब पूरी होने से ‘रह’ जाती है। किसी से मोहब्बत
में ‘रह’ जायें तो दिल की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं।
दिल से दिल की बात कहने के मायने बदल जाते हैं क्योंकि कहने वाला ‘दिल’ भी अपना होता है और सुनने वाला ‘दिल’ भी। जिसके दिल की बातें हैं, बस वही पास नहीं होता। जब ऐसा होता है तो दिल के पास केवल दो ‘ऑप्शन’ होते हैं।
या तो बहुत खुश हो ले। या फिर बहुत रो ले। अपने आंसू हैं। किसी और को तो दिखाये नहीं जायेंगे।
कोई उन्हें समझेगा भी क्या? क्यों?
मैं भी किसी को क्या समझाऊंगी? क्यों समझाऊंगी?
कि?
क्यों हैं ये आंसू ?
ख्वाहिशों का मतलब मैं शादी के बाद ही समझी थी।…शादी के बाद….
50% जिंदगी
शादी अच्छे से हो गई। शादी के बाद संजीव के साथ दिल्ली आ गई। ख्वाहिशों ने अभी भी पूरी तरह से सिर नहीं उठाया था। शायद जरूरत महसूस नहीं हुई थी। कभी-कभी जिन्दगी बिना ख्वाहिशों के ही सब कुछ देती है। मुझे लगा मिल रहा है।
एक घर… छोटा था, मगर हम दोनों के समाने के लिए काफी था।
मैं खुश थी क्योंकि अपना था वो घर। अपने घर के अहसास भी अपने होते हैं। अपने से मतलब यह नहीं कि खरीदा हुआ या किराए का। मैं मकान की बात नहीं कर रही। मैं घर की बात कर रही हूं। अपना मतलब हम दोनों की दुनिया का।
आधा उससे था। आधा मुझसे।
हम दोनों से मिल कर वो पूरा होता था।
अक्सर लव मैरिज के बारे में सुनती थी तो सोचती थी कि यह ‘लव’ क्या होता है? इसे कैसे करते हैं? लड़के-लड़कियां जो साथ घूमते फिरते हैं। उनमें जो ‘लव’ फैक्टर होता है वो आखिर होता क्या है?
रोमांस?
उसके बारे में तो मैंने सिर्फ सुना ही था या फिल्मों में देखा था। रियेल लाईफ में वो कैसा होता है इसका मुझे जरा भी आभास तक ना था। पहली बार संजीव ने छुआ तो जिस्म में अजीब सी मीठी सी
झुरझुरी दौड गई।
‘लव’ में दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांसें तेज हो उठती हैं, ऐसा सिर्फ सुना था, लेकिन आज ‘लव’ ‘लाइव’ था तो महसूस भी कर लिया था।
एक लड़का-लड़की जब ‘लव-फीलिंग’ के साथ ‘एक साथ’ होते हैं तो उनमें प्यार की वो कशिश क्या होती है, आज पता चल गई थी।
टाईडल वेव जो समुद्र में आती हैं, वो शरीर में भी वैसे ही आती हैं। आती हैं। जाती हैं। फिर से आती हैं। फिर से जाती हैं। आना जाना लगा रहता है।
क्यूं भला? चली ही क्यूं नहीं जातीं या हमेशा के लिए ही आ क्यूं नहीं जातीं? चले जाकर फिर ना
आना या आकर रुके रहना दोनों ही मुमकिन जो नहीं।
क्यूं किसी के ऐसे छूने पर मन यह चाहता है कि वो छुअन कभी खत्म ना हो।
क्यूं मन चाहता है कि वह पल हमेशा बने रहें।
“अरे! क्या हुआ? जरा सा छूते ही तुम तो ऐसे सिमट गई जैसे छुई मुई की पत्तियां।” संजीव ने जैसे छेड़ा था मुझे । सचमुच मैं उसके छूने से सिमट सी गई थी। हाथ वापस खींचने की कोशिश की।
मैं खामोश थी।
“लगता है नारी को शर्म से सिमट जाने की अदा छुई मुई से ही मिली है?”
“शर्म दोनों की ‘नेचर’ होती है और दोनों में होती है… इसलिए तो।”
“इसलिए शायद शहरों में छुई मुई नहीं होती?” उसके इन शब्दों में गहराई थी। कुछ पल के लिए जैसे वो कहीं खो गया था। शहरों की लड़कियों के ‘फॉरवर्ड’ होने की बातें तो मैंने भी सुनी थीं। पर शायद संजीव उस माहौल से कुछ अलग नेचर का था। उसे गांव की गौरी पसंद आ गई थी। अपनी-अपनी
पसंद है।
“मुझे तुम्हारी यह बात अच्छी लगी।”
“आं…! कौन सी?”
“यही कि शर्म दोनों की नेचर होती है और दोनों में होती है।”
“आपने यह क्यों कहा कि शहरों में छुई मुई नहीं होती?”
“ओपन माईडेड लोग हैं। सब कुछ ओपन है।”
“शर्म भी?”
“शायद। मेरी समझ सारी दुनिया की समझ नहीं हो सकती। ऐसा मैं समझता हूं। औरों की समझ की बात नहीं कर सकता। हो सकता है जो लोग इस ओपन सोसायटी का हिस्सा हैं उन्हें ऐसा ना लगता
हो और उनके लिए सब कुछ नॉर्मल ही हो।
अगर कोई फाईव स्टार स्वीमिंग पूल में जाकर डुबकी लगाता है तो दोबारा भी ऐसा करना उसके लिए कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगा। लेकिन रोजाना घर के बाथरूम में नहाने वाला तो जरुर सोचेगा कि वहां सबके सामने कपड़े उतारूं कि नहीं? मीन्स… शर्म फैक्टर।”
संजीव के इस प्रकार के विश्लेषण पर मैं मुस्करा दी थी। संजीव की सादगी की कायल भी हुई थी।
खुद को लक्की समझ रही थी कि वो मुझे मिला।
75% जिंदगी
संजीव बिजनिस में थे।
बिजनिस बढ़ रहा था इधर जिम्मेदारियां भी। वक्त बीत नहीं रहा था, वो तो जैसे भाग रहा था। वक्त के हर पल में खुशियां हों तो वक्त की फिक्र किसे होती है। उसे पूछता कौन है?
चुनती थी, यहां खुशियां चुन रही थी।
इंसान उन खुशियों को ही समेटने में लगा रहता है। मैं भी तो वही कर रही थी। गांव में थी तो फूल
मैं किसी रेस ट्रैक पर नहीं थी फिर भी लगा कि भाग रही हूं।
लेकिन मेरा यह भागना मुझे अच्छा लग रहा था। जिन्दगी जब इस तरह से हिरण की तरह कुलांचे
भरते हुए भागती है तो उसे भागते देखना अच्छा लगता है।
लेकिन मैं भूल रही थी कि भागने के साथ एक फैक्टर और भी जुड़ा है।
रुकना |
भागने वाले को कहीं जाकर रुकना पड़ता है। अपनी गति थामनी होती है। हमेशा तो कोई भागते नहीं
रह सकता।
और।
रुकने से पहले गतिमान चीज की गति कुछ कम होती है।
वो समय आता हुआ लगा मुझे। निशांत और प्रशांत अब आठ और नौ साल के हो चुके थे। अचानक
संजीव ने दिल्ली से बाहर बिजनिस बढ़ाना डिसाईड किया।
यह अच्छा था लेकिन मेरे लिए मुश्किल ।
मन जब कहीं किसी के या अपने ही डिसीजन पर अटकता है तो मुश्किलें या उनकी सम्भावनायें नजर आती हैं।
मुश्किल कहां थी?
मुझे निशांत और प्रशांत के साथ वहीं रहना था। दिल्ली में। उनके फ्यूचर का सवाल था। दिल्ली में
अच्छे स्कूल थे। अच्छी एजुकेशन थी।
लेकिन अकेली जिन्दगी?
संजीव के बिना कैसे रह पाऊंगी? शहरों की जिन्दगी में मैं ज्यादा रची-बसी नहीं थी। उससे ज्यादा
वाकिफ नहीं थी। उसकी ज्यादा अभ्यस्त नहीं थी। मानसिक रूप से भी नहीं।
आदमी सारा दिन बाहर रहे। चौबीस घंटे होते हैं एक रात और दिन में। वो दो घंटे के लिए भी घर आ
जाये तो ‘कॉन्फिडेंस’ बना रहता है।
औरत को अपनी और परिवार की सुरक्षा का अहसास रहता है। और सुरक्षा की बात न भी करूं तो भी मेरी लाईफ में से कुछ कम होने जा रहा था, खुद से उसे कैसे मैनेज करती?
किसी के जाकर लौट आने की उम्मीदें भी काफी होती हैं। उम्मीदें टूटर्ती हैं तो जिन्दगी में इन्तजार पसर जाता है। सुबह जाकर शाम को लौटने का इंतजार ही मुश्किल होता है तो अब इन्तजार की घड़ियां बेहद लम्बी होने वाली थीं।
कुछ दिन । कुछ रातें।
कितने दिन? कितनी रातें?
उस रात बेडरूम में मैं संजीव के सीने पर सिर रख कर उसके बहुत पास तक सिमटी हुई थी। लग रहा था जैसे यह ‘नजदीकियां’ मुझसे अब ‘छिनने’ वाली हैं।
संजीव से ‘दूरियों’ की ‘नजदीकियां’ अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस करके मेरी आंखों में आंसू थे। पलकों से अभी गिरे नहीं थे। उनको ना गिरने देने के बहाने शायद खुद को हौंसला देना चाहती थी।
“क्या तुम रुक नहीं सकते?”
“समझा करो प्रिया जाना जरूरी है।”
“क्यों जरूरी है?”
“लगता है अभी कुछ किया नहीं। कुछ करना है।”
“जितना कर रहे हो उससे भी हमारी लाईफ आसानी से चल सकती है।”
“ये सच है कि बिजनिस के मामले में पच्चीस पैसे से पचास पैसे पर तो आया हूं लेकिन मुझे रुपए
तक पहुंचना है।”
‘फिर लाईफ ‘पच्चीस पैसे’ पर रुक जायेगी!”
“मतलब?”
“मैं बिजनिस की बातें नहीं जानती संजीव। मैं जिन्दगी को जानती हूं। जिन्दगी भी तो उसी पर्सेटेज के
हिसाब से चलती है।”
“मैं अभी भी नहीं समझा।”
“अगर मैं कहूं कि जिन्दगी के मामले में मैं भी पच्चीस पैसे से पचास पैसे पर तो आई हूं लेकिन मुझे
भी रुपये तक पहुंचना है तो वो तुम्हारे बिना मुझे कैसे मिलेगी?”
“मतलब तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें हण्ड्रेड पर्सेट लाईफ दूं। मतलब तुम्हें हण्ड्रेड पर्सेट साथ दूं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारी जिन्दगी को पच्चीस पैसे से रुपया बनाने में तुम्हारे साथ कम्प्रोमाईज करू?”
“हां! जिन्दगी में साथ, प्यार और सहारे की भी जरूरत होती है। धंधे के साथ कंधे की भी जरूरत होती है। और ये कम्प्रोमाईज नहीं है। शरीर से सांस छूट जाये तो शरीर सड़ने लगता है। ये जरूरत है कि शरीर और सांस दोनों एक साथ रहें।”
“दुनिया में एक और बड़ी जरूरत भी है प्रिया। अपनी महत्वाकांक्षायें। और पैसा तो है ही। वैसे तो मैं यह भी सोचना नहीं चाहता फिर भी चलो अगर सोचूं कि मैं ‘टॉप’ इण्डस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकता लेकिन बनने का महत्वाकांक्षी तो हो सकता हूं। और मेरी महत्वकांक्षा तभी पूरी होगी जब मैं इस तरफ कोई कदम उठाऊंगा। अगर सभी तुम्हारी तरह सोचने लगें तो इस दुनिया में ‘टॉप’
इण्डस्ट्रियलिस्ट पैदा होने ही बंद जायेंगे। फिर यह सब किसके लिए करूंगा? तुम लोगों को बेहतर जिन्दगी देने के लिए ही ना?”
“यानी एक को कुर्बानी देनी होगी?”
“तुम पहेलियां बहुत बुझा कर बातें कर रही हो?”
“या तो हमारी जिन्दगी पच्चीस पैसे से रूपए पर पहुंचेगी या तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं?”
“इसे कुर्बानी मत समझो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिये। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं।”
“मैं ‘मेरी’ नहीं, हमारी जिन्दगी’ की बात कर रही हूं लेकिन तुम सिर्फ अपनी इच्छाओं के पूरा होने की बात कर रहे हो। मैं जो चाहती हूं उसमें हम कम से कम साथ तो रहेंगे लेकिन तुम जो चाहते हो उसमें वहां तुम अकेले हो यहां मैं अकेली ।”
“मैं महीनों के लिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा। बीच-बीच में आता-जाता रहूंगा।”
“तुम मुझे सिर्फ ‘अपनी’ उम्मीदों के सहारे छोड़ रहे हो। मैं ‘तुम्हारे’ अहसासों के साथ जीना चाहती हूं।
मुझसे यह अहसास मत छीनो ।”
“और अगर मैं जिन्दगी में ही ना रहूँ तो? तो भी तो जियोगी मेरे बिना?”
“संजीव” बांध टूट गया था। आंसू बह निकले थे।
“तुम मेरी सांस हो प्रिया। मेरी जिन्दगी हो। तुम मुझसे या मैं तुमसे दूर नहीं हूं।”
मैं जानती थी कि संजीव का प्यार मेरे लिए कम नहीं है, लेकिन शायद मेरी हसरतें… पास रहने की,
अहसासों में जीने की, मुझे मुश्किलों में डाल रही थीं।
लेकिन मेरी हसरतें मेरा स्वार्थ तो नहीं थीं। मैं ‘सेल्फिश’ नहीं थी।
मेरी हसरतों में हम दोनों साथ थे। अपने-अपने हिस्से की पर्सनली, प्रोफेशनली, फैमिलियर
जिम्मेदारियों के साथ ।
क्या इन सभी जिम्मेदारियों में ‘प्यार’ को निभाने की जिम्मेदारी प्रेफरली नहीं होनी चाहिये?
या फिर इकोनोमिकली जरूरतें मजबूर कर रही हों कि जाना जरूरी लगे। लोगों को दूर जाना पड़ता है।
जाते हैं। वहां ‘जिन्दगी को पच्चीस पैसे पर भी छोड़ कर जाना जरूरी होता है। मगर!
यहां ‘जाना’ जरूरत नहीं, ‘जीना’ जरूरत थी।
संजीव नहीं रुके थे। ना ही मैं रोक पाई थी।….
100% जिंदगी
मैं समझ गई थी कि मुझे अकेले जीने की आदत डालनी होगी।
जिन्दगी अब मेरे लिए मौसम की तरह थी। मौसम के कई रूप और रंग होते हैं।
पतझड | बसंत बहार। बारिश सूखा । सर्दी। गर्मी।
अकेले रहते हुए मैं इन सब को झोल रही थी। संजीव यहां पास नहीं होते थे तो पतझड़ महसूस करती थी।
उनके आने की खबर मेरे लिए बसंत का रूप थी। उनका आ जाना बहार। उनका दिख जाना बारिश । पास रहते हुए दूरी सर्दी। उनका स्पर्श गर्मी उनका फिर से चले जाना सूखा।
एक रात फिर से मैं संजीव के साथ थी।
वही बेडरूम था।
वही मैं थी।
वही वो थे।
मैंने कहावत सुनी थी। एक चुप सौ सुख ।
मगर कितना चुप?
कब तक चुप?
“मैं सोचती हूं संजीव कि पैसे के साथ जिन्दगी का भी आना जरूरी होता है। पैसा तो फिर भी बचा सकते हैं लेकिन जिन्दगी को… उसके हर पल को बचा कर रखना लगभग नामुमकिन होता है। जिन्दगी तो हर पल में तेजी से खर्च होती चली जाती है। और इसे कमाया नहीं जा सकता।” संजीव के पास मेरी ऐसी बातों का कोई जवाब नहीं होता था या वो देना नहीं चाहता था। बिस्तर पर जहां उनकी जगह थी, वहां उनके रहते कभी सलवटें नहीं थीं। या यूं कहूं कि उनकी मौजूदगी में कभी सलवटें दिखी नहीं वहां।
अब रहती थीं।
मैं उस खाली जगह को अपनी मुट्ठियों में भींच कर उनके होने का अहसास करती थी। मेरी इन बेचैन कोशिशों से चादर सलवटों से भर जाती थी।
पास ही खाली पड़े तकिये पर सिर रख देती थी। उनकी मौजूदगी का अहसास कहां होता था? आंखें रो लेती थीं। तकिये पर सूख चुके आंसूओं की ना जाने कितनी बूंदों के निशान बन गये थे।
पर उन्हें अब देखने वाला कौन था?
कमरे में कितना भी अँधेरा हो मगर अहसास हैं तो दिख ही जाते हैं। अब सब कुछ चला गया था। रौशनी में भी अंधेरे महसूस होते थे। उनमें अकेले रहने की मजबूरियां ।
आंखें बंद रखो या खुली उनमें रौशनियों की चमक गायब थी।
जीने की मजबूरियों ने अपनी दीवारें इतनी ऊंची कर ली थी कि झॉक पाना भी मुश्किल हो रहा था कि उनके पीछे कोई एक दिल भी है।
आज सब कुछ फीका था, भाव फीके, हंसी फीकी, मुस्कान फीकी, गहरा कुछ था तो चेहरे पर आने से छुपाया जाता तनाव, जिसने चेहरे की रंगत को भी फीका कर दिया था, हंसी तो खुल कर आती है, ख़ुशी तो खिल कर आती है, पर तनाव खिलखिलाहटों को खुलने नहीं देता, मकड़ी की तरह झपटता है, और दबोच लेता है आपने जाल में खिलखिलाती ख़ुशी को, उसका तेज चूस जाता है, तब हंसी शव के समान निस्तेज, नजर आती है, होंठ हंसने की चेष्टा में, फैलते तो हैं मगर हंस नहीं पाते हैं, तनाव हंसता जान पड़ता है, तनाव भारी पड़ता है जब, प्यार अपने प्यार को नहीं पाता है।।
अपने दिल की भावनायें जैसे रेत हो गई थीं। आंधियों में रेत उड़ा करती है। इतनी रेत कि कुछ दिखाई नहीं देता। आंधियों में कहीं भी देखने की कोशिश करोगे तो रेत के नन्हें नन्हें कण आंखों में जाकर चुर्भेगे।
जिन्दगी है। जैसी और जब तक जीने को मिलेगी, जीना पड़ेगी।
मैंने कहां गलत कहा था कि प्यार जिस्म और सांस की तरह होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सांस के बिना जिस्म की और जिस्म के बिना सांस की क्या अहमियत रहेगी?
जिस्म को सांस से या सांस को जिस्म से दूर कर दोगे तो सांस में जिन्दगी होने के बाद भी वो मरने लगेगी और जिस्म भी कहां जिन्दा रहेगा?
जब सोचते हैं अपने बारे में, अपने लिए, किसी लम्हा, हर लम्हा ये सोचते हैं, कि… दिन में जैसी
चाहत की चाहत है, वैसी क्यों हासिल नहीं, लम्हे तो सोचने के लिए ही होते हैं, हर लम्हा सोचते हैं. कि मुहब्बत, जिसका असर ‘दिल’ से ‘आंखों’ तक है, वैसी क्यों हासिल नहीं, क्यों रोती हैं आंखें बेबसी के आंसू, उमंगें… उन्हें क्यों हासिल नहीं, हालात ही ऐसे हैं या, अपनी सोचों का असर है, फिर सोचते हैं कि, क्यों ना इस चाहत को वैसा ही अपना लें, जैसी वो हासिल है, क्यों उसे हालातों की दलदल में अपना दम घोंटने दें, मुहब्बत तो मुहब्बत है, चाहे जैसी सही।।
कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे मैं एक दुकान हूं, जहां से कोई महीने भर का राशन भरने आता है। फिर महीने भर तक उसका पता नहीं चलता। यह राशन कभी जल्दी खत्म हो जाता है कभी कुछ और देर में खत्म होता है लेकिन दुकान पर ‘फिर’ आयेगा कोई इसके पूरी तरह खत्म होने के बाद ही।
बच्चे अब बड़े हो चुके हैं।
संजीव अभी भी मौसम की तरह मेरी जिन्दगी में आते हैं।
मेरे हिस्से का हजारों पों का प्यार चंद पलों में ही सिमट गया था। मुझे लगता है अपने हिस्से का प्यार तो मैने पाया ही नहीं। संजीव से जितना पाया था वो मेरी कोख ने उसे दो बेटों के रूप में वापस लौटा दिया था।
मैं यह नहीं कहती कि प्यार खत्म हो गया है। प्यार की इच्छायें खत्म हो गई हैं।
अब तो समझौते हैं।
जिन्दगी दुकान की तरह चलती रहेगी।
कब तक?
यह कौन जानता है?
अब खुद को ढाला है खुद अपने ही सहारे ।
मेरा दिल है। दिल से दिल की बातें हैं और हसरतों के दाग हैं जिन्हें धोना है।
समाप्त !!



